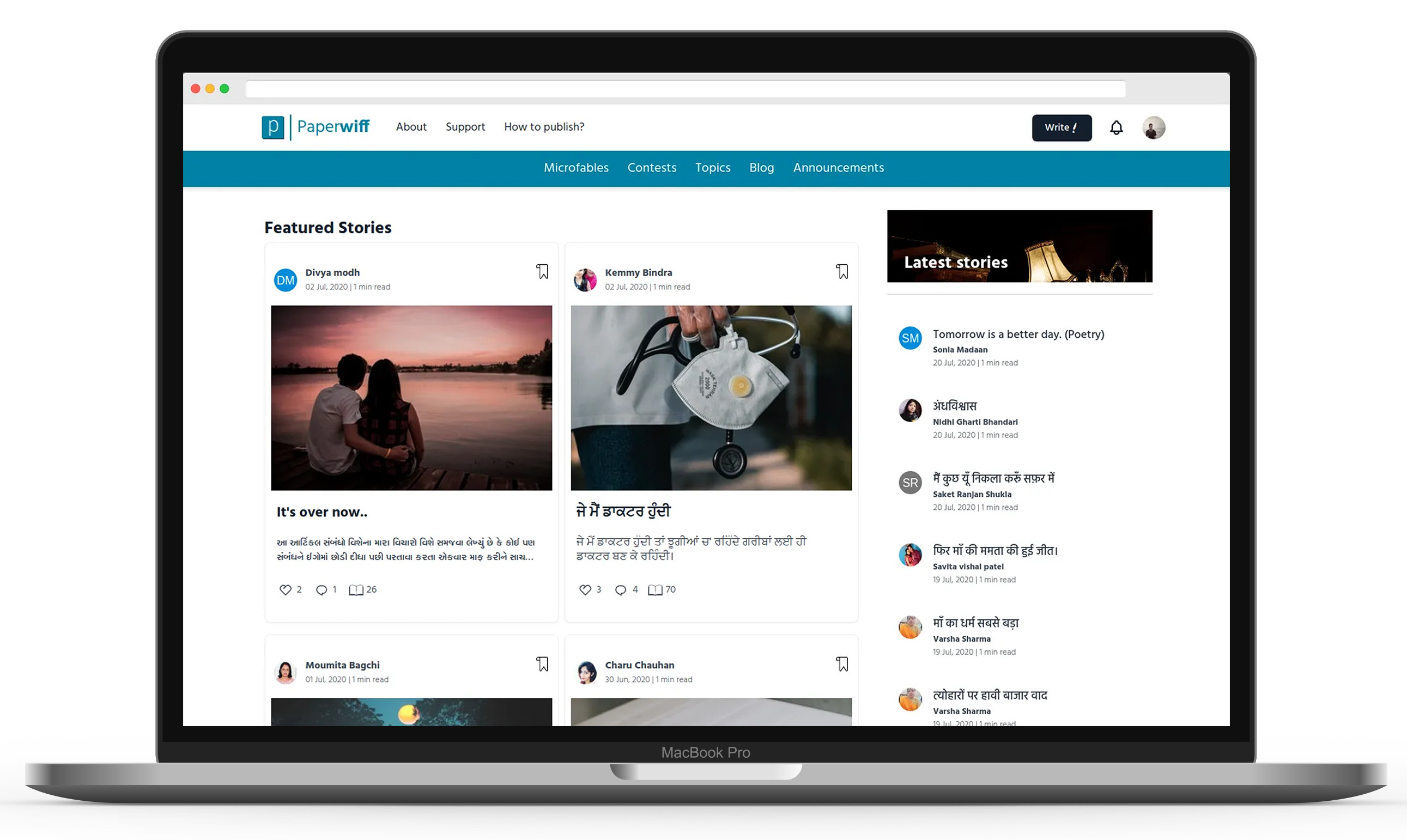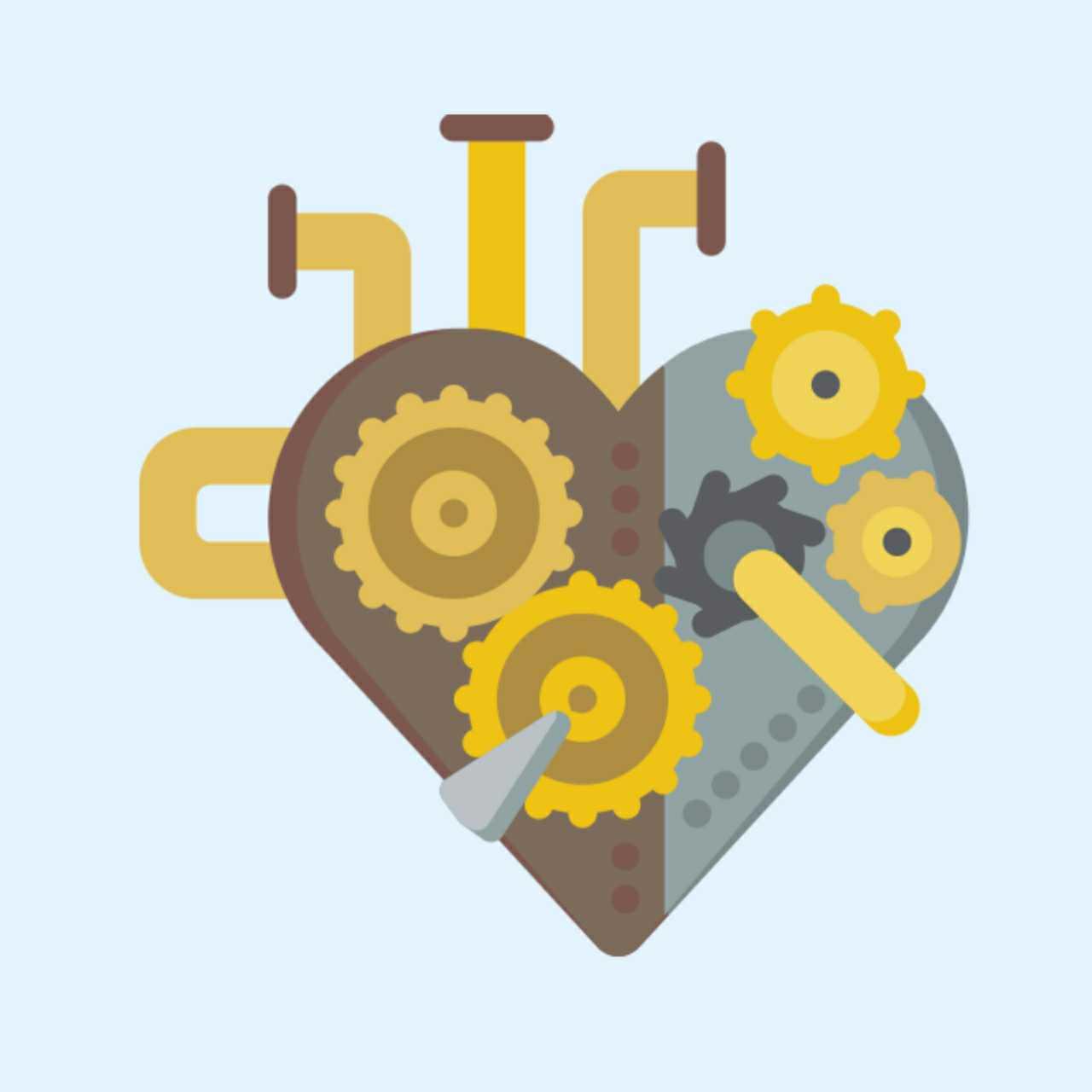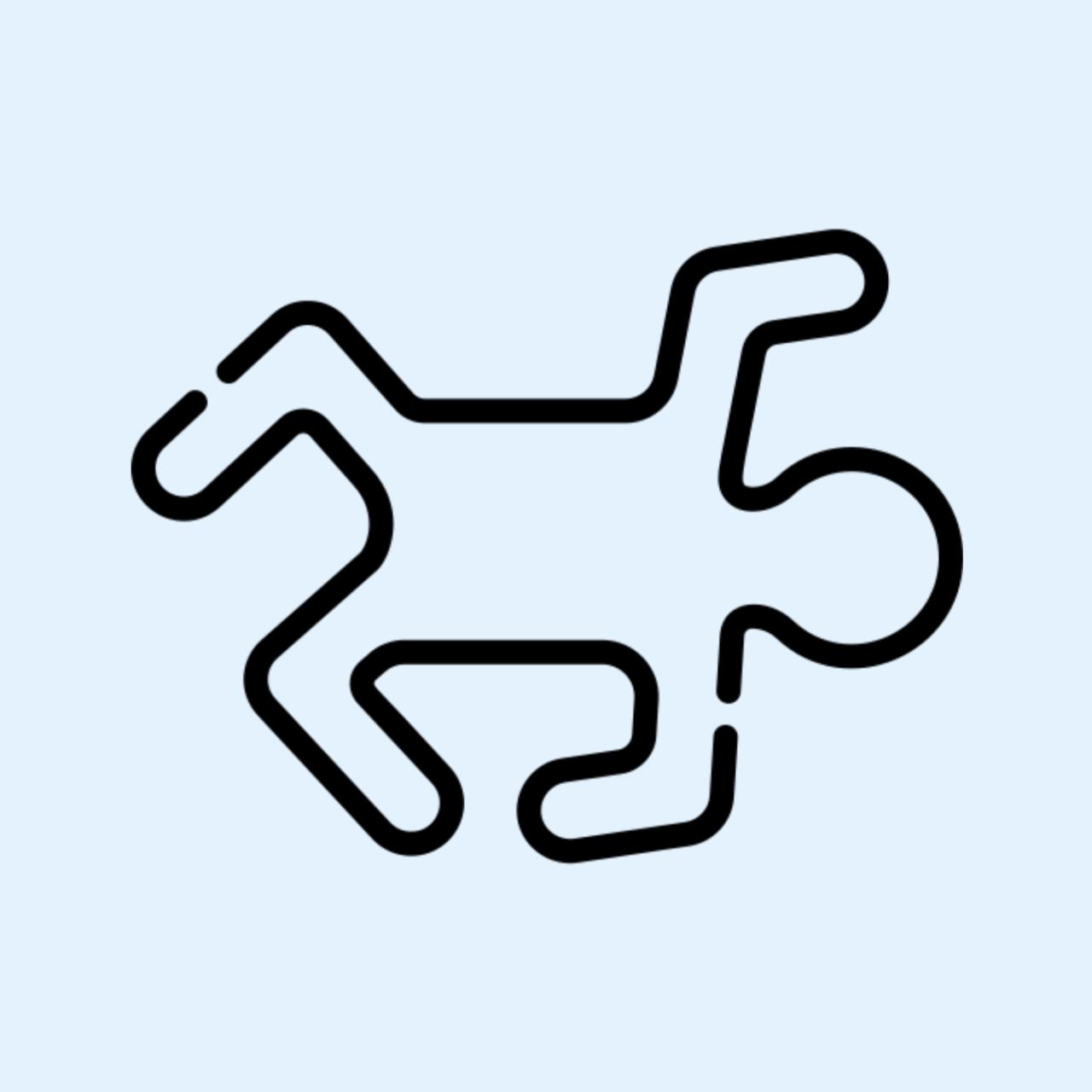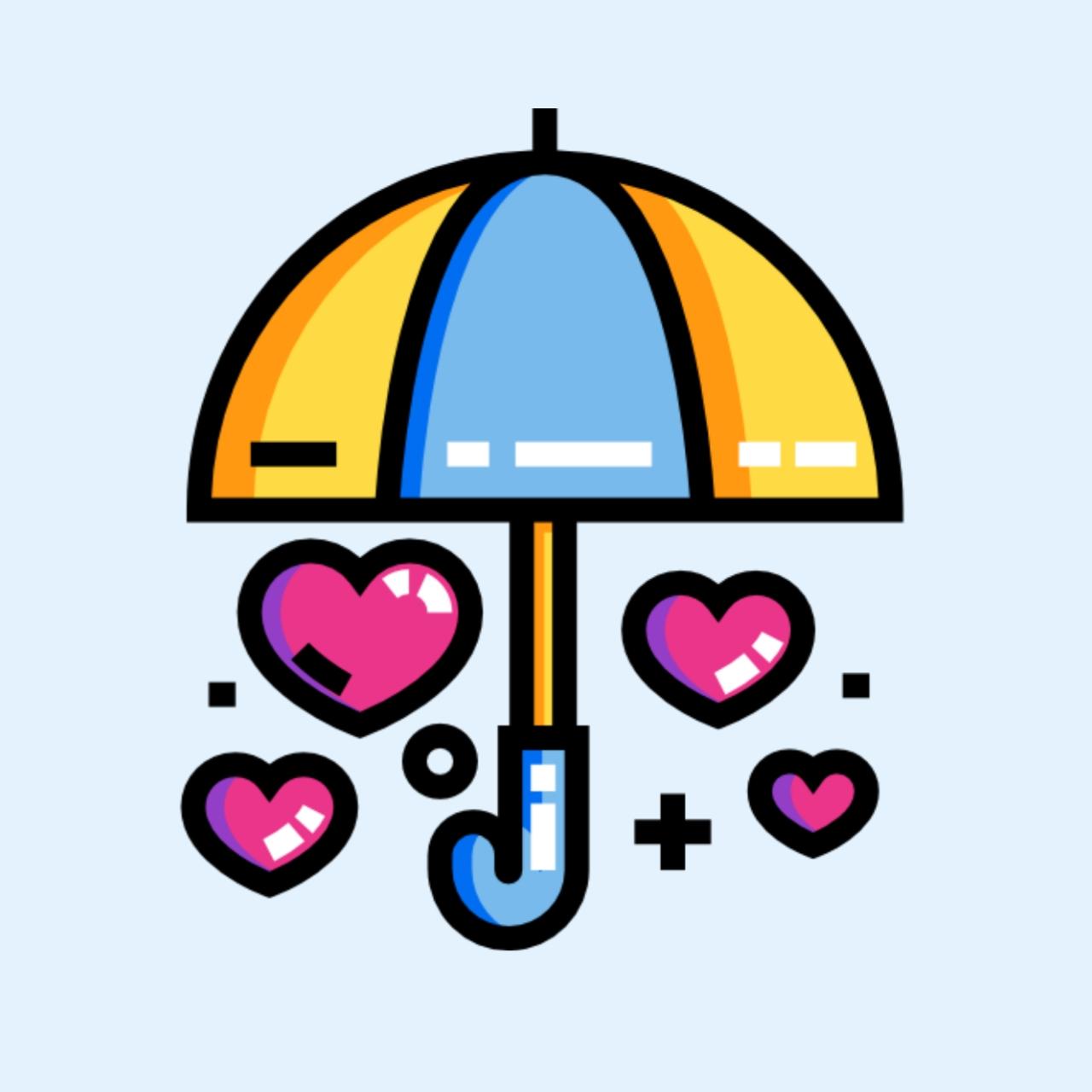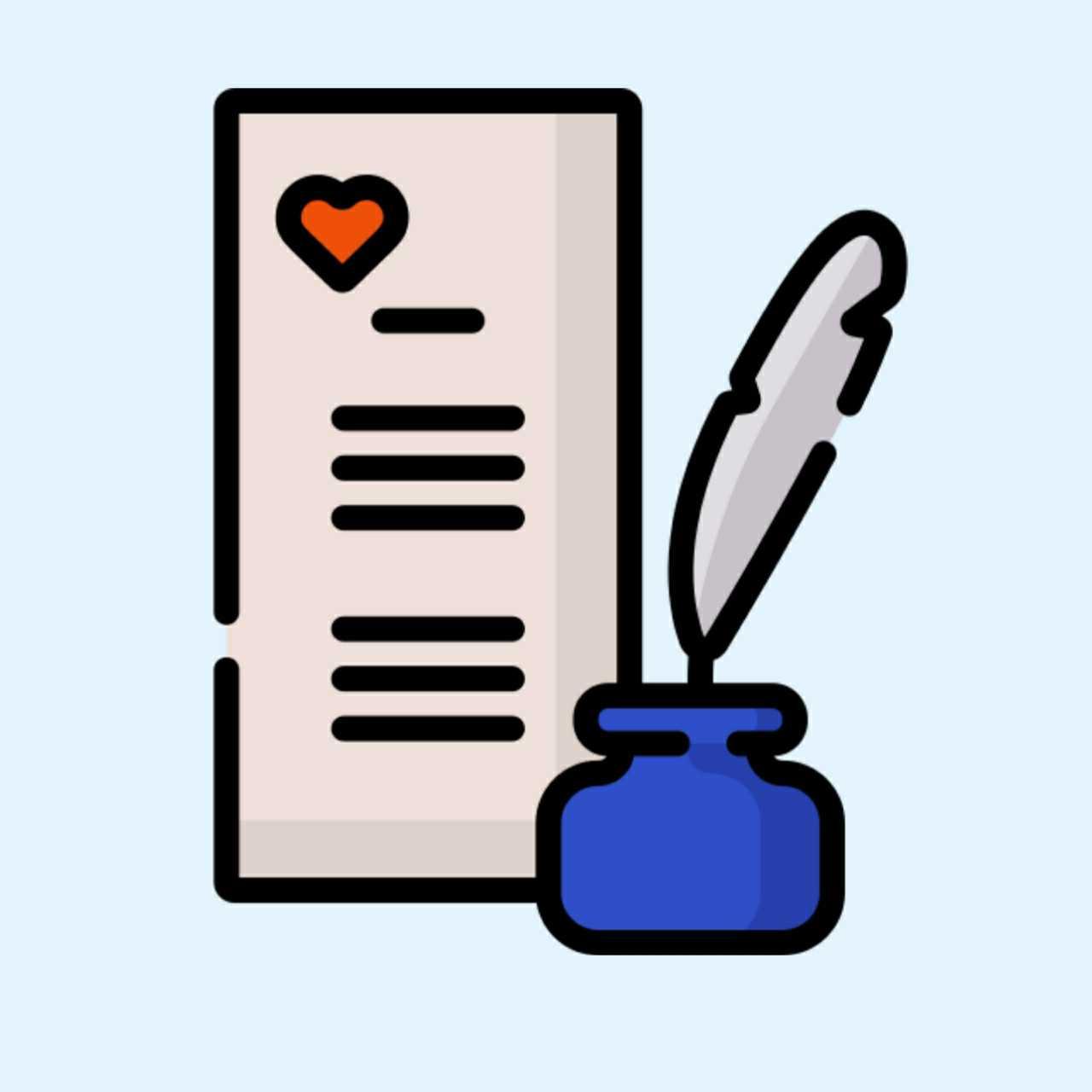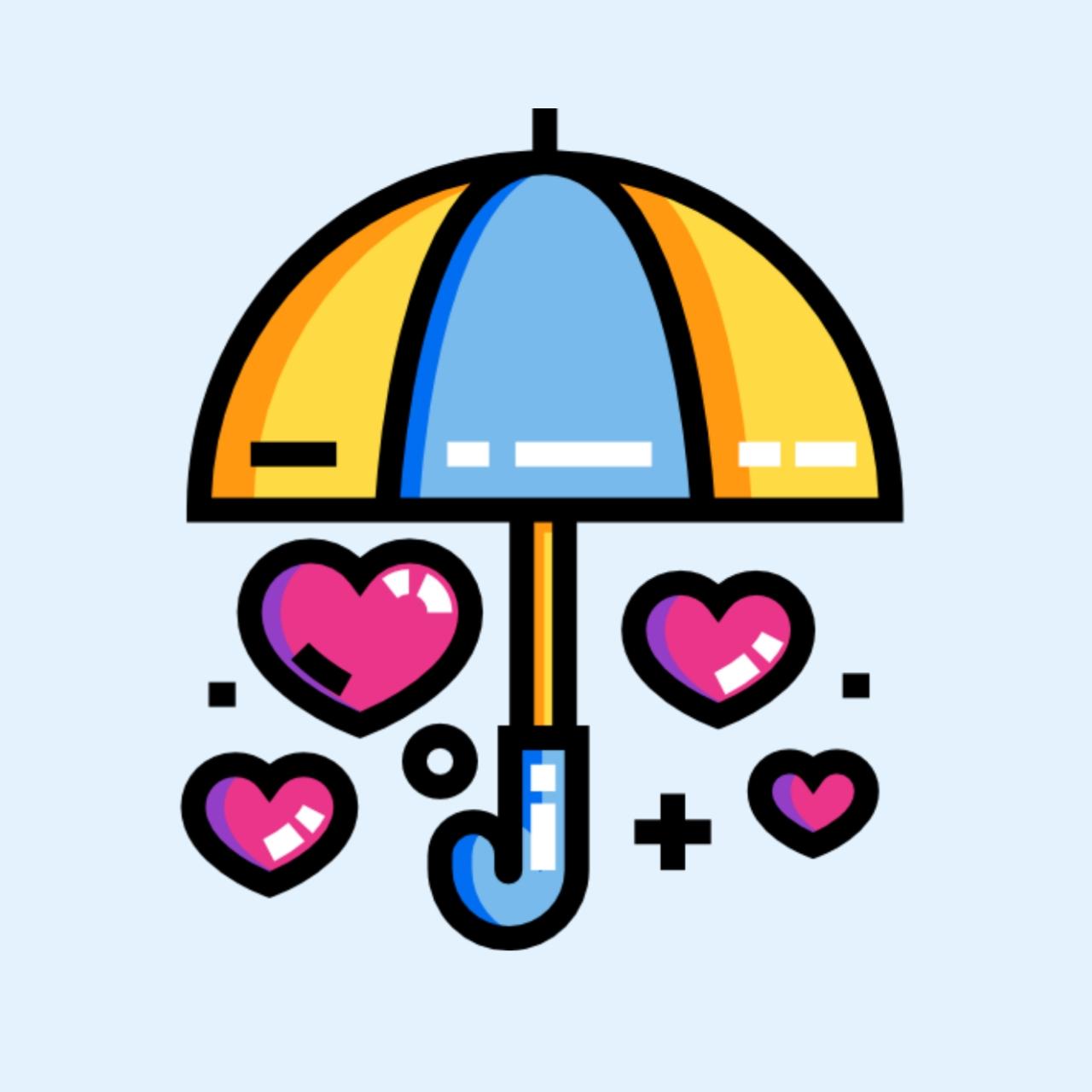Everything you need. Nothing you don't.
We provide you with just enough features to create content, share it with your readers, and publish it into a beautiful blog.
-
Distraction free editor
Write your posts/tutorials on paperwiff. Easily add images, lists, quotes, codeblocks, and more in our intuitive easy to use editor.
-
Multi-Shot quotes
Show your design and writing skills by grouping your work into Microfables. Get unlimited access to images worldwide which suits your quote.
-
Writing Community
You own everything you write, Be a part of the biggest vernacular writing community and get the chance to discuss the real writer issues.
-
Fast and friendly support
Our 24/7 support team always goes an extra mile to ensure you are having an excellent experience using Paperwiff. Our team is just a Send button away.
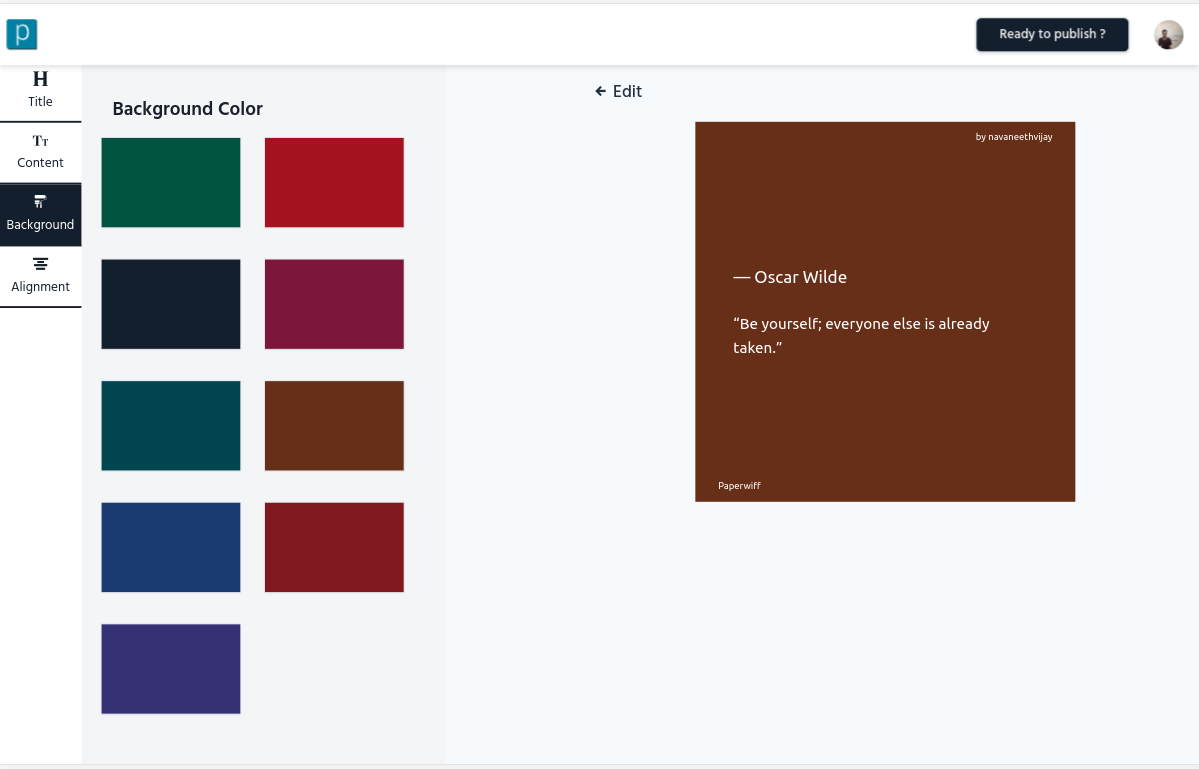
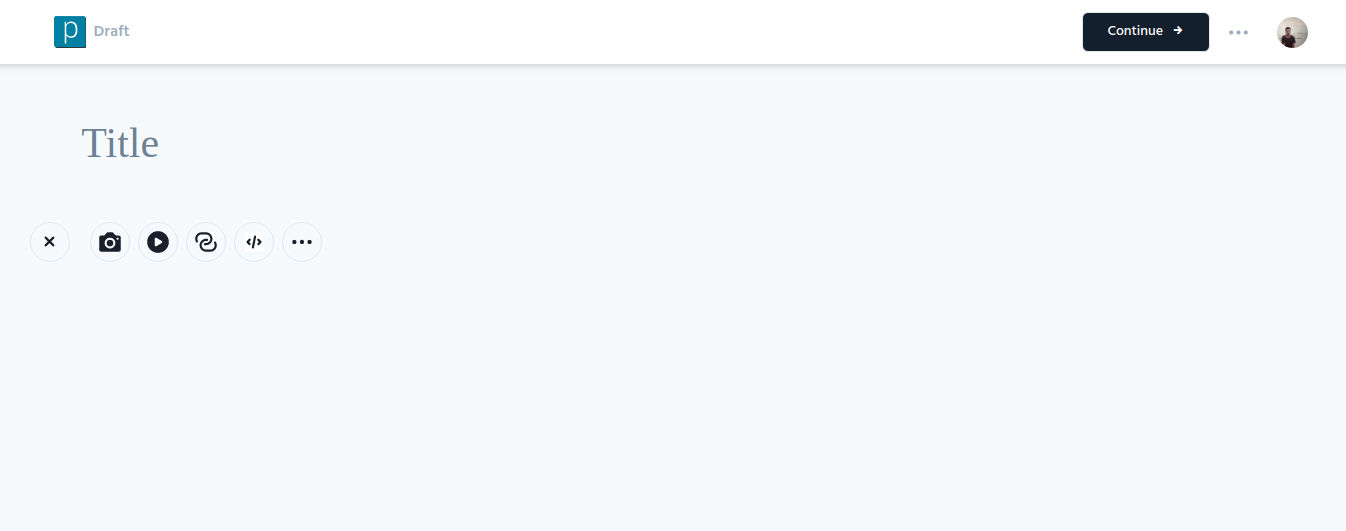
"Read to learn, write good for recognition in return, write best to earn, endorse your language for a magical turn".
ಕನ್ನಡ
Kannada
हिन्दी
Hindi
ਪੰਜਾਬੀ
Punjabi
മലയം
Malayaam
বাংলা
Bengali
ગુજરાતી
Gujarati
اردو
Urdu
मराठी
Marathi
தமிழ்
Tamil
తెలుగు
Telugu
“More than 22 Indian languages and counting”
Become a smart reader and an earning writer today!
Already have an account? Login
Explore the subjects of your interest.
view allGrowing family of 9000+ curious readers, 5000+ contemporary writers envisioning the revival of 4000 languages of India.
Recent stories
Everyday 10's of stories are posted on paperwiff